“आम लोगों व किन्नरों” मृत नैतिकताओं का समाज
“भिलाई स्मृति नगर चौकी के चंद्र नगर कोहका में आम लोगों व किन्नरों के बीच जमकर ईंट पत्थर और लात घूंसे चले। ” क्या किन्नर आम लोग नहीं है ? यह कैसी खबर छाप कर अखबार किन्नरों को अलग बताने में लगे हुए है ? यह एकलौती ऐसी खबर नहीं है , हाल ही में न डी टीवी और इंडिया टुडे ने एक ट्रांसमैंन को औरत बताते हुए खबर छापी थी I
ऐसा पहली बार नही हुआ है। और ना ही मैं ऐसा ही कह सकनें की स्थिति में हूँ कि ये अंतिम बार होगा। प्रत्येक दिन में न जाने कितनी बार ऐसा होता है जब किसी बात का स्पष्टीकरण खोज पाना या उस बात का समर्थन कर पाना, अपनी हत्या कर देने के समान कष्टकर प्रतीत होता है।
हमारी ‘आम” या ‘नॉर्मल’ होने की परिभाषाएँ इतनी क्रूर,इतनी भयावह क्यूँ हो जातीं हैं? क्यूँ ऐसा है कि अपने बीच खोदी हुई इन जानलेवा खाइयों को हम भरना ही नही चाहते? जो जैसा है,वैसा रहे, परवर्तन भूल से भी न होने पाएँ, रुका हुआ पानी रुका रहे, सड़ जायें, महामारियाँ फैल जाएँ, लोग मरने लगें, सभ्य समाज सड़ाँध मारने लगे, सभ्यता नष्ट हो जाए लेकिन बस परिवर्तन ना हो! कोई पत्ता न हिल जाए, कोई कहीं साँस न ले ले…
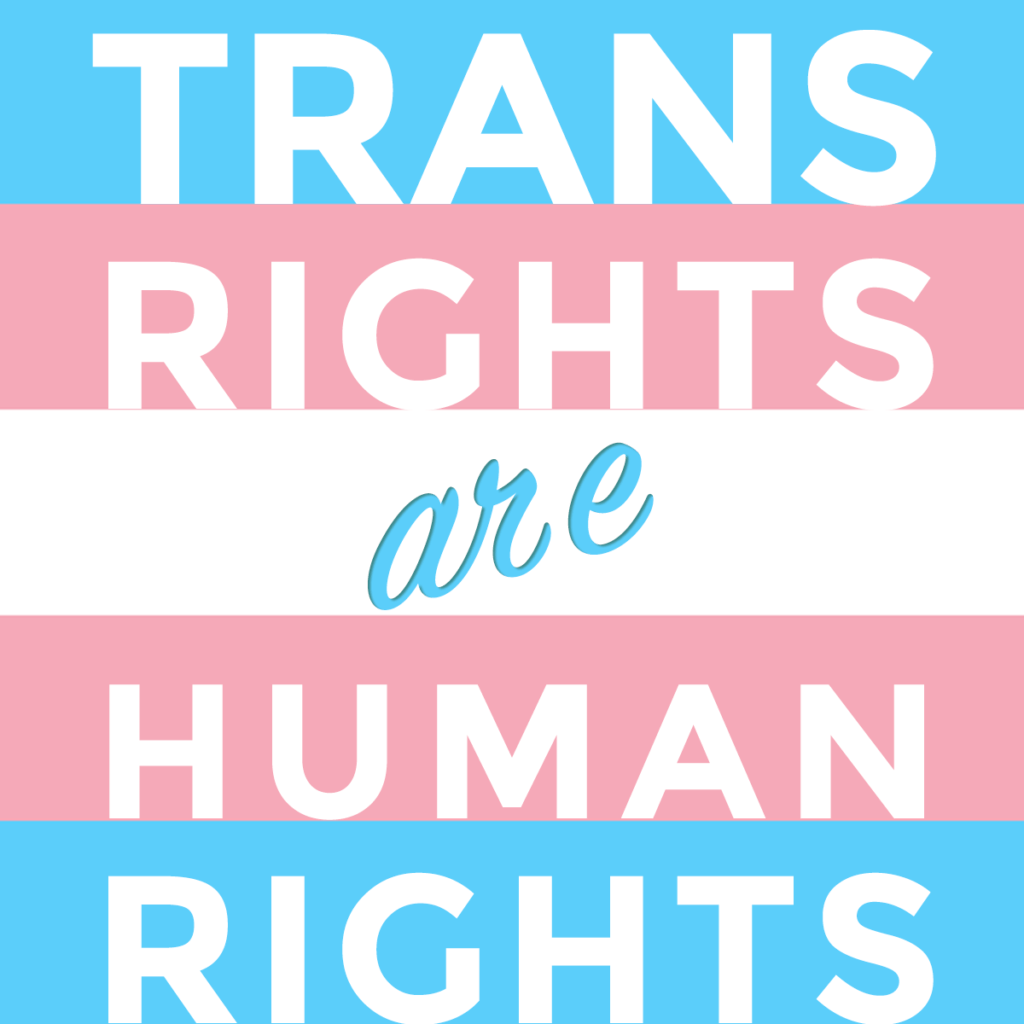
क्या सच में हम आज भी वहाँ तक पहुँच पाएँ हैं कि स्वयं को श्रेष्ठ कह पाने की जुर्रत कर सकें!
विशेष रूप से अगर मैं कहूँ तो हिन्दी पट्टी का समाज कब अपनी खोखली नैतिकताओं से बाहर आ पाएगा! इस प्रश्न का उत्तर देने में मुझे लगता है कि कई-कई सदियाँ भी कम पड़ेंगी। आने वाले सौ वर्षों के बाद के समाज की कल्पना कर पाना कम से कम मेरे लिए तो संभव नही है।
ट्रांसजेंडरों को सभ्यता की शुरुआत से लेकर आज इस इक्कीसवीं सदी तक, मनुष्य होने के बावजूद अपने मनुष्य होने के अधिकारों के लिए लड़ना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है। और आश्चर्य की बात ये है कि एक समाज के रूप में हमनें, अपनी इस क्रूरता पर, दूसरों से घृणा करने वाली इस संस्कृति पर कभी अपराधबोध या शर्मिंदगी महसूस नही की।
ऐसा क्यूँ होता है कि अँधेरों में ट्रांसजेंडरों को भूखी नज़रों से देखने वाला, उनके बलात्कार करने वाला,उन्हें नोचने पीटने वाला सभ्य समाज, उजालों में उनकी उपस्थिति तो छोड़िए, उनके जिक्र से ही असहज हो जाता है।
हमारे परिवार,हमारा समाज इतना महान है कि एक ट्रांसजेंडर बच्चे के लिए उनके घरों में,परंपराओ में, संस्कृति में, प्यार में,वात्सलय में कोई स्थान नही है। अपने स्त्री या पुरुष होने के मानकों में फिट बैठाने के सारे प्रयास कर लेने के बाद, ऐसे संस्कारवान समाज के, संस्कारवान माता पिता उन्हें घरों से उठा कर फेंक देते हैं। और इसके साथ ही यह सुनिश्चित हो जाता है कि उन्हें उनके कथित सभ्य समाज के किसी भी कोने में कोई स्थान प्राप्त न होने पाए।
अपने आस पास, गली-मोहोल्लों में कुछ ट्रांसजेंडरों के रहने से, उनके जीवन जीने की कोशिश से समाज क्यूँ विचलित है? क्या ये कथित आम लोग इस बात से भयभीत हैं कि आम होने की परिभाषा से वंचित कर दिए गए ये लोग उनकी ओढ़ी गई महानता का नकाब खींच कर रख देंगे!
कैसी विडम्बना है कि मनुष्य होकर, दूसरे मनुष्यों से हमनें मनुष्य होने के अधिकार छीन लिए हैं।
जब लोग कहते हैं कि भारत के ट्रांसजेडरों की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है, बहुत बदलाव आयें हैं, तब एक बार यकीन करने की इच्छा होती है। लेकिन तभी जब हिन्दी के इतने प्रतिष्ठित अखबार “आम लोगों और किन्नरों” जैसी भाषा का उपयोग करते हैं तब सारे यकीन सूखे पत्तों की तरह पैरों तले कुचले जाते हुए महसूस होते हैं। एक कलम जिसे समाज का मार्गदर्शक होना चाहिए, उससे समाज के साथ-साथ सड़ जाने की बू आती है। खैर जब मनुष्यों में ही संवेदनशीलता मर चुकी हो तब एक कलम से उसकी उम्मीद करना हास्यास्पद ही लगता है। लेकिन हँसने का साहस कहाँ बाकी रह गया है!
भास्कर , हरिभूमि तथा जो अख़बार ऐसी भाषा का प्रयोग कर किन्नर समुदाय को इंसान भी नहीं मान रहे है उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए , जिस तरह यह खबर लिखी गयी है , उस से ट्रांस्फोबिअ को बढ़ावा मिल रहा है I
news source : https://www.bhaskar.com/local/chhattisgarh/durg-bhilai/news/there-was-a-dispute-over-the-issue-of-vacating-the-house-the-brick-and-stone-went-fiercely-130327095.html
Image via outrightinternational.org



